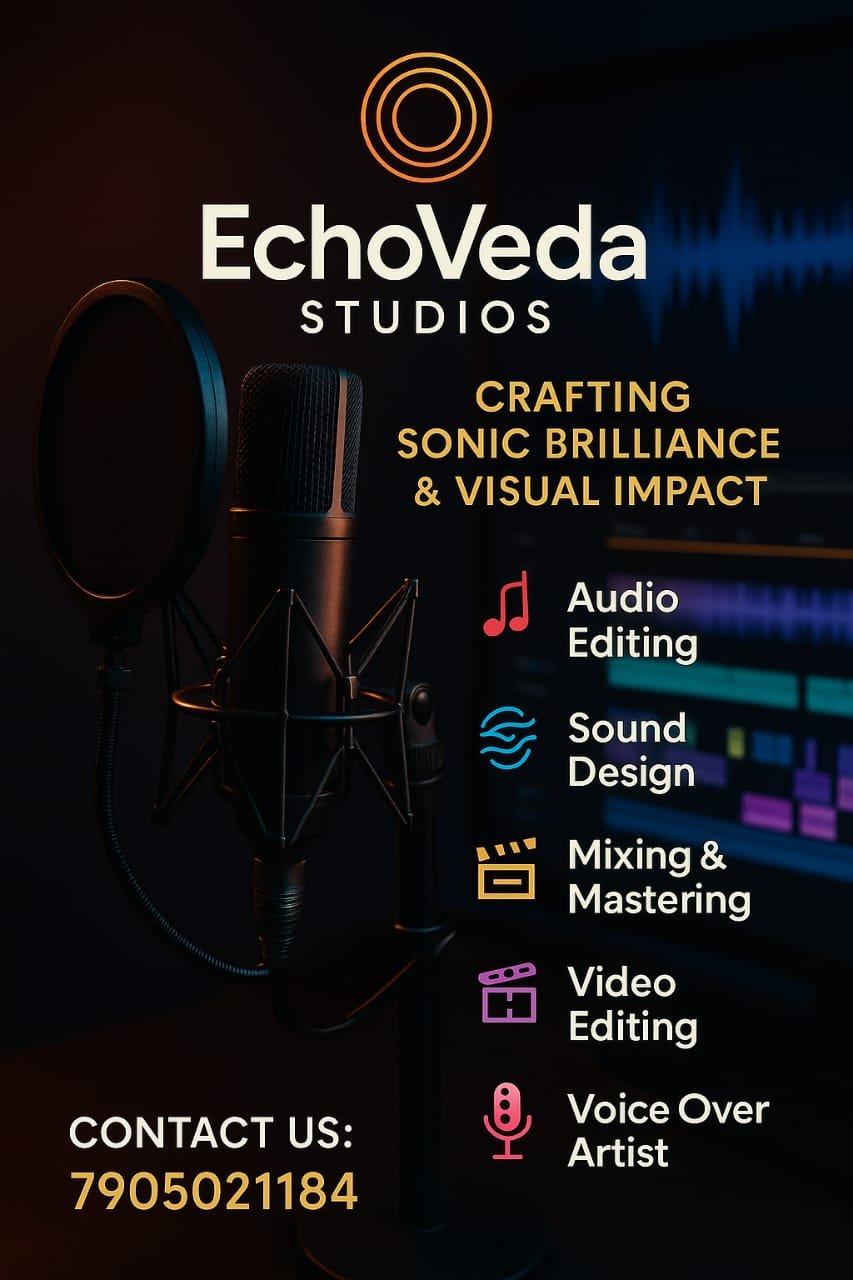भारत का लचीलापन: 27 साल पहले अमेरिकी प्रतिबंधों से कैसे उबरा

- Khabar Editor
- 28 Aug, 2025
- 99323

Email:-infokhabarforyou@gmail.com
Instagram:-@khabar_for_you

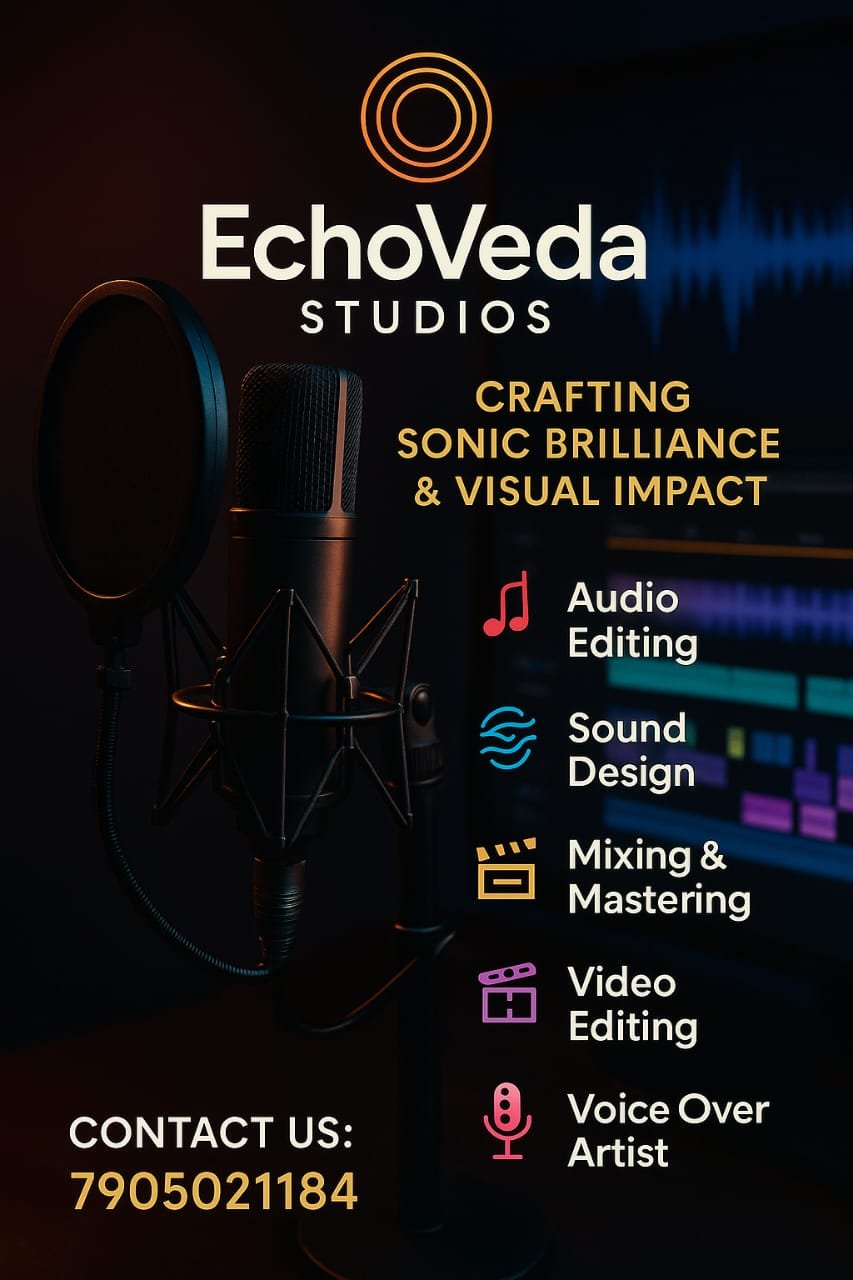
दशकों से, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों, सहायता में कटौती और शुल्कों सहित आर्थिक उपायों का इस्तेमाल करता रहा है। हालाँकि, ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि भारत ने न केवल इन दंडात्मक कार्रवाइयों का सामना करने, बल्कि इनसे उबरकर एक मज़बूत, अधिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ गहरे रणनीतिक संबंधों के साथ उभरने की उल्लेखनीय क्षमता लगातार दिखाई है। कूटनीतिक कौशल और स्वदेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता में निहित यह लचीलापन, द्विपक्षीय संबंधों में एक आवर्ती विषय है, जैसा कि 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद और हाल के शुल्कों के संदर्भ में सबसे प्रमुख रूप से देखा गया है।
Read More - गणेश चतुर्थी: भारत पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों और भक्ति के साथ गणेशोत्सव मना रहा है
भारत के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे कठोर उदाहरण 1998 में पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से किए गए ये परीक्षण वैश्विक परमाणु व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थे, और अमेरिका ने कड़े उपायों के साथ जवाब दिया। इनमें सभी गैर-मानवीय विदेशी सहायता को समाप्त करना, विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का विरोध, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा रक्षा हार्डवेयर की बिक्री पर प्रतिबंध शामिल थे। उदारीकरण-पूर्व युग में, ऐसी कार्रवाइयाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती थीं। हालाँकि, 1991 के सुधारों से पहले से ही मज़बूत भारत की अर्थव्यवस्था, अनुमान से कहीं अधिक लचीली साबित हुई।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विद्रोही लेकिन व्यावहारिक रुख अपनाया। वाजपेयी के सार्वजनिक बयानों में भारत के "संसाधनों और आंतरिक शक्ति के विशाल भंडार" पर ज़ोर दिया गया, जो राष्ट्रवादी भावना से मेल खाता था। हालाँकि प्रतिबंधों ने अल्पकालिक बाधाएँ पैदा कीं, जैसे कि अवरुद्ध ऋणों के कारण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में देरी, लेकिन रणनीतिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा उनके दीर्घकालिक प्रभाव को कम किया गया। विडंबना यह है कि प्रतिबंधों ने भारत के लिए परमाणु और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को तेज़ करने में उत्प्रेरक का काम किया। भारत ने इस अवसर का उपयोग अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए भी किया।
राजनयिक परिदृश्य भी भारत के पक्ष में बदल गया। प्रतिबंधों के बावजूद, वाशिंगटन के साथ संचार के रास्ते खुले रहे। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब क्लिंटन प्रशासन ने पहली बार पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का खुलकर पक्ष लिया। इसने वाशिंगटन में भारत के सामरिक महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाया। यह कूटनीतिक गर्मजोशी 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऐतिहासिक भारत यात्रा के साथ पराकाष्ठा पर पहुँची, जो दो दशकों में पहली ऐसी यात्रा थी, जिसने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। बुश प्रशासन के दौरान, आतंकवाद-निरोध और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में साझा हितों के कारण, ये संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। इस कूटनीतिक बदलाव का अंतिम प्रमाण 2008 का भारत-अमेरिका परमाणु समझौता था, जिसने भारत के परमाणु अलगाव को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया और विस्तारित रक्षा सहयोग एवं व्यापार सहित एक पूर्ण रणनीतिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया।
ट्रम्प प्रशासन द्वारा दंडात्मक शुल्क लगाने के साथ, भारत के लचीलेपन की परीक्षा आज फिर हो रही है। रूस से तेल खरीदने के भारत के संप्रभु निर्णय पर दबाव डालने के उद्देश्य से लगाए गए ये शुल्क, आर्थिक उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं। हालाँकि ये अल्पावधि में कपड़ा और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, भारत एक बार फिर अपने निर्यात बाज़ारों का विस्तार करके और घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके इसका जवाब दे रहा है। जैसा कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है, "इन वैश्विक चुनौतियों से भारत को पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले साहसिक सुधारों के लिए प्रेरित होना चाहिए।" वर्तमान स्थिति, 1998 की तरह, एक झटके के रूप में नहीं, बल्कि भारत के लिए अपने आर्थिक और राजनयिक संबंधों में और विविधता लाने और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के अवसर के रूप में देखी जा रही है।
समाचार के मुख्य बिंदु
- भारत का ऐतिहासिक लचीलापन: लेख में तर्क दिया गया है कि भारत के पास प्रतिबंधों और शुल्कों सहित अमेरिकी आर्थिक दबाव पर काबू पाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, और वह लगातार मज़बूत होकर उभरा है। इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक आवर्ती चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- 1998 के प्रतिबंध: सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 1998 में भारत के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य विदेशी सहायता में कटौती, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों को अवरुद्ध करके और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाकर भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था।
- वाजपेयी का दृष्टिकोण: यह समाचार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद दृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण रुख अपनाया और भारत की आंतरिक शक्ति और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया।
- प्रतिबंध उत्प्रेरक के रूप में: लेख में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिबंधों ने, यद्यपि अल्पकालिक आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किए, भारत के स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता के लिए उत्प्रेरक का काम किया। इसने आयात निर्भरता को कम करने और परमाणु एवं रक्षा क्षेत्रों में घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति प्रदान की।
- राजनयिक बदलाव: प्रतिबंधों के बावजूद, राजनयिक रास्ते खुले रहे। संबंधों में नरमी आने लगी, विशेष रूप से 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया। इसके परिणामस्वरूप 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा और राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ, 2008 के परमाणु समझौते के साथ संबंधों में पूर्ण पुनर्स्थापन हुआ।
- वर्तमान संदर्भ: लेख 1998 की स्थिति और डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा हाल ही में लगाए गए शुल्कों के बीच तुलना करता है। ये शुल्क भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना जारी रखने के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप लगाए गए हैं।
- भारत की वर्तमान रणनीति: नए टैरिफ के जवाब में, भारत एक बार फिर आत्मनिर्भरता की इसी रणनीति का अनुसरण करते हुए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- आर्थिक मजबूती: लेख में बताया गया है कि 1991 के उदारीकरण से प्रेरित भारत की अर्थव्यवस्था 1998 में लचीली थी और तब से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रतिबंधों के दौरान भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मज़बूत रही और बाद के वर्षों में इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई।
- विशेषज्ञ टिप्पणी: लेख में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जैसे विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ शामिल हैं, जो वर्तमान टैरिफ को भारत के लिए "बड़े सुधारों" को लागू करने और दीर्घकालिक विकास एवं लचीलापन सुनिश्चित करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं।
समाचार के उप-बिंदु
A. 1998 के प्रतिबंध: एक निर्णायक क्षण
- उपायों की गंभीरता: ये प्रतिबंध भारत पर लगाए गए अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंधों में से थे। ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी प्रतिबंधों सहित अपने लक्षित क्षेत्रों में व्यापक थे।
- विशिष्ट प्रभाव:
विदेशी सहायता: अमेरिका ने आर्थिक विकास सहायता में लगभग 2.1 करोड़ डॉलर और ग्रीनहाउस गैस कार्यक्रम के लिए 60 लाख डॉलर की सहायता राशि समाप्त कर दी।
अंतर्राष्ट्रीय ऋण: अमेरिका ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले ऋणों का सक्रिय रूप से विरोध किया, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए अनुमानित 3-4 अरब डॉलर का वित्तपोषण अवरुद्ध हो गया।
- रक्षा और प्रौद्योगिकी: प्रतिबंधों ने रक्षा हार्डवेयर, सेवाओं और विदेशी सैन्य वित्तपोषण की बिक्री को निलंबित कर दिया, जिसका सीधा असर कारगिल युद्ध से ठीक पहले भारत की रक्षा क्षमताओं पर पड़ा।
- अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक प्रभाव: हालाँकि प्रतिबंधों के कारण कुछ परियोजनाओं में अस्थायी मंदी और द्विपक्षीय व्यापार में मामूली गिरावट आई, लेकिन वे समग्र अर्थव्यवस्था को पंगु नहीं बना पाए। 1991 के उदारीकरण सुधारों ने पहले ही एक मजबूत और स्थिर आर्थिक आधार तैयार कर दिया था।
B. सुधार का मार्ग और रणनीतिक साझेदारी
- घरेलू प्रतिक्रिया: प्रतिबंधों ने आत्मनिर्भरता के लिए एक मज़बूत प्रयास को बढ़ावा दिया। भारत, जिसके पास पहले से ही एक मज़बूत संस्थागत अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक आधार था, ने स्वदेशी परमाणु और रक्षा प्रौद्योगिकियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह औपचारिक "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम से पहले की बात है।
- आर्थिक विविधीकरण: भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों में सफलतापूर्वक विविधता लायी, विभिन्न वस्तुओं के लिए यूरोपीय संघ, रूस, जापान, चीन और मध्य पूर्वी देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का प्रभाव कम हुआ।
- कूटनीतिक सफलताएँ:
कारगिल युद्ध (1999): अमेरिका ने संघर्ष के दौरान भारत का साथ दिया, जो उपमहाद्वीप के प्रति उसकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था।
क्लिंटन की यात्रा (2000): इस यात्रा ने संबंधों में एक प्रतीकात्मक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने परमाणु परीक्षणों के बावजूद भारत के साथ सहयोग करने की अमेरिका की इच्छा का संकेत दिया।
9/11 के बाद का सहयोग: आतंकवाद-निरोध में साझा हितों ने बुश प्रशासन के तहत संबंधों को और मज़बूत किया। अमेरिका ने सितंबर 2001 में 1998 के शेष प्रतिबंधों को हटा दिया।
2008 का परमाणु समझौता: यह ऐतिहासिक समझौता कूटनीतिक प्रयासों का अंतिम परिणाम था, जिसने अमेरिका को भारत को परमाणु तकनीक बेचने और गैर-एनपीटी स्थिति के बावजूद भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत करने की अनुमति दी।
C. वर्तमान चुनौती और भविष्य का दृष्टिकोण
- नए टैरिफ: यह लेख ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए नए टैरिफ को अमेरिकी आर्थिक दबाव के एक समकालीन उदाहरण के रूप में उजागर करता है। ये टैरिफ रूसी तेल पर भारत के रुख की प्रतिक्रिया हैं।
- प्रभाव और प्रतिक्रिया: हालाँकि टैरिफ से विशिष्ट क्षेत्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है, भारत का नेतृत्व इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देख रहा है। जैसा कि अधिकारियों और विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है, भारत का मजबूत घरेलू बाजार, मजबूत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विशाल विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण बफर प्रदान करते हैं।
- रणनीतिक अनिवार्यता: लेख का निष्कर्ष है कि भारत एक बार फिर चुनौती को अवसर में बदलने के लिए तैयार है। अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने और आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, नई दिल्ली का लक्ष्य दबाव के इस मौजूदा दौर से और भी बड़े विजेता के रूप में उभरना है।
Business, Sports, Lifestyle ,Politics ,Entertainment ,Technology ,National ,World ,Travel ,Editorial and Article में सबसे बड़ी समाचार कहानियों के शीर्ष पर बने रहने के लिए, हमारे subscriber-to-our-newsletter khabarforyou.com पर बॉटम लाइन पर साइन अप करें। |
| यदि आपके या आपके किसी जानने वाले के पास प्रकाशित करने के लिए कोई समाचार है, तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें: 8502024040 |
#KFY #KFYNEWS #KHABARFORYOU #WORLDNEWS
नवीनतम PODCAST सुनें, केवल The FM Yours पर
Click for more trending Khabar

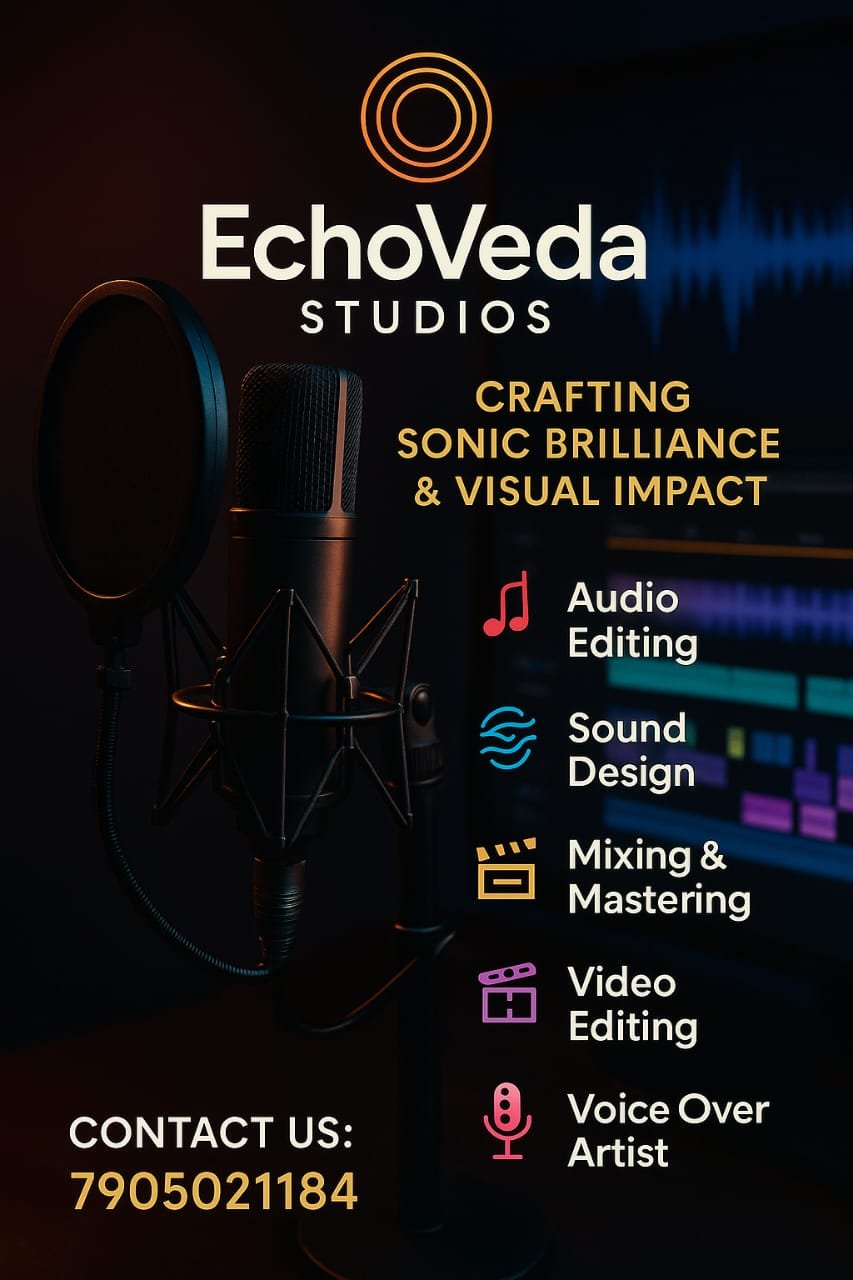
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Search
Category