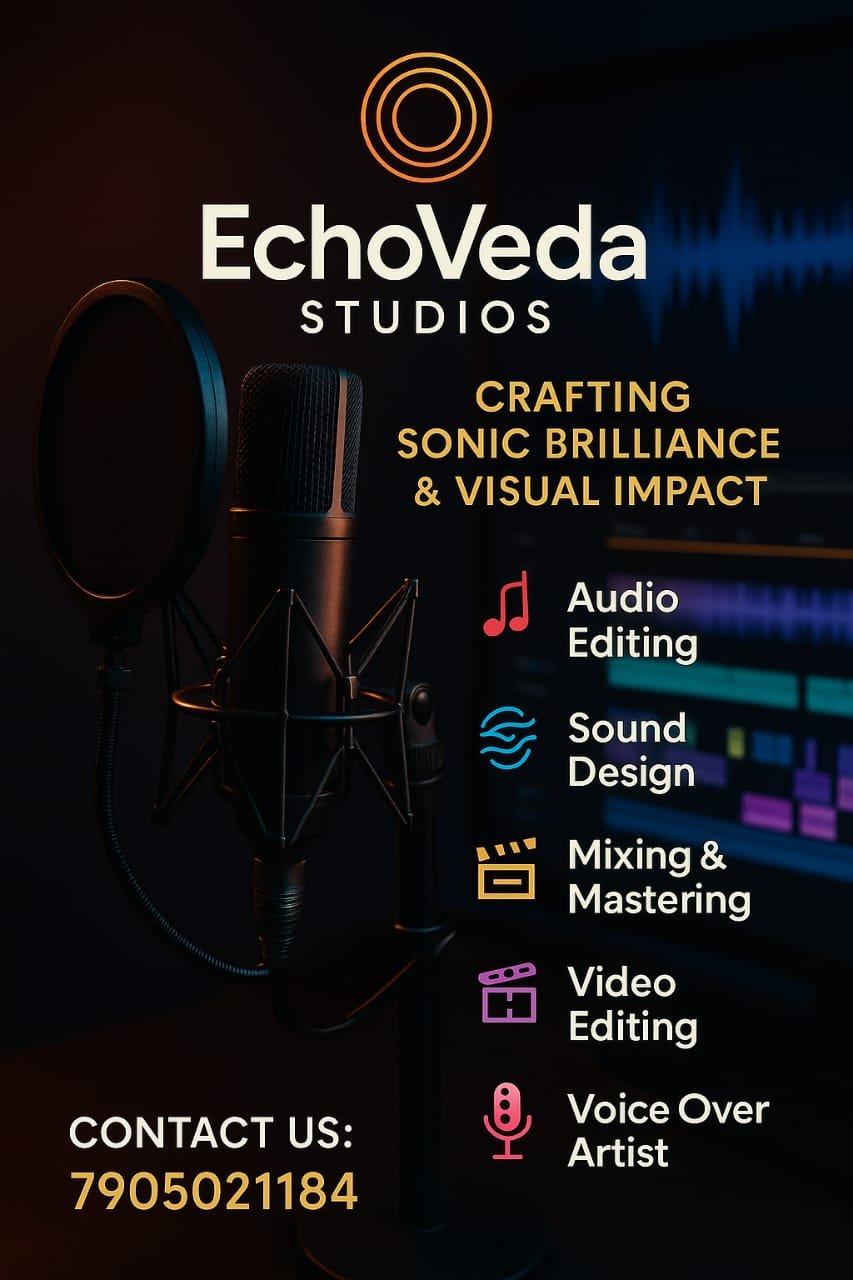भारतीय संविधान में प्रस्तावना से परे धर्मनिरपेक्षता को समझना
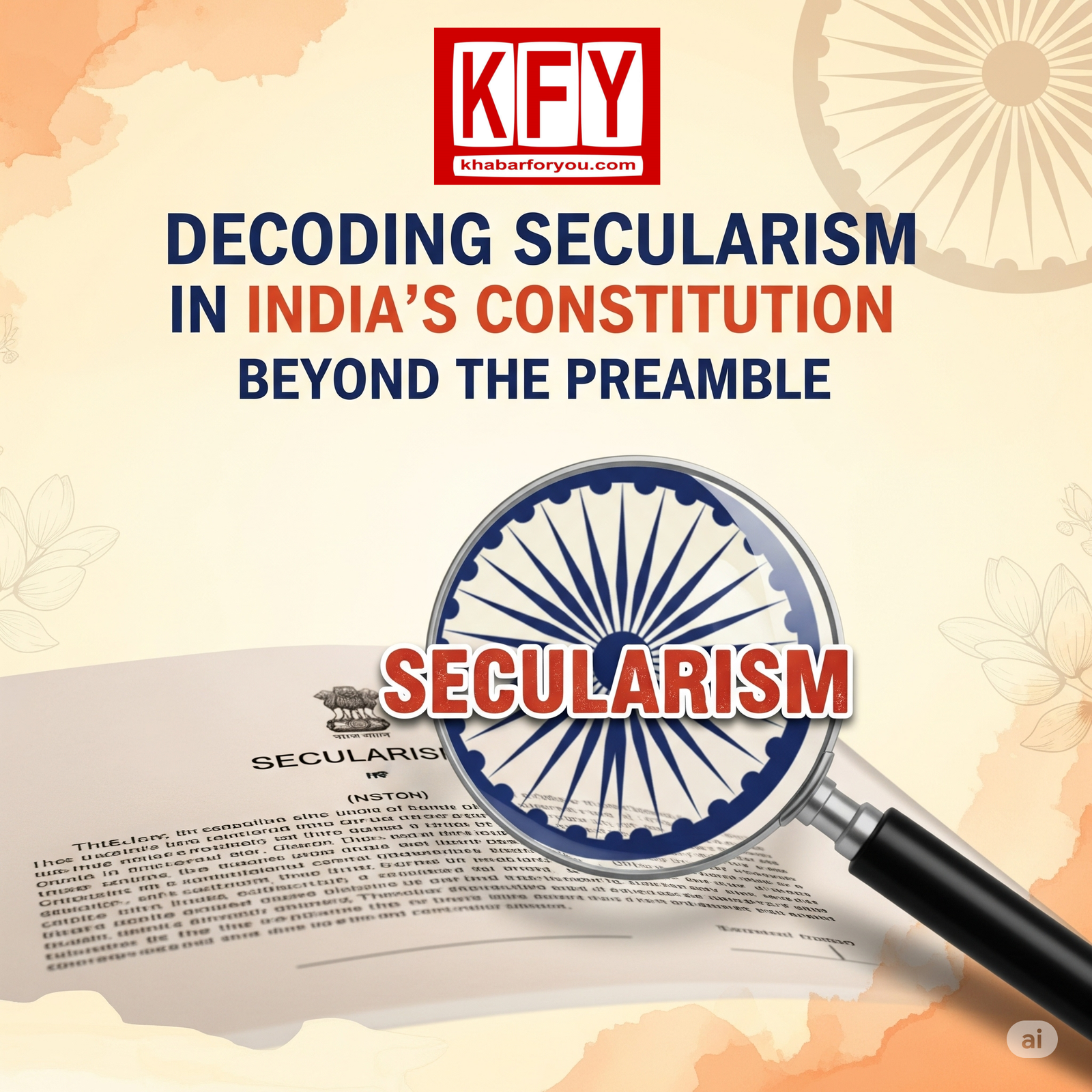
- Khabar Editor
- 01 Jul, 2025
- 98826

Email:-infokhabarforyou@gmail.com
Instagram:-@khabar_for_you

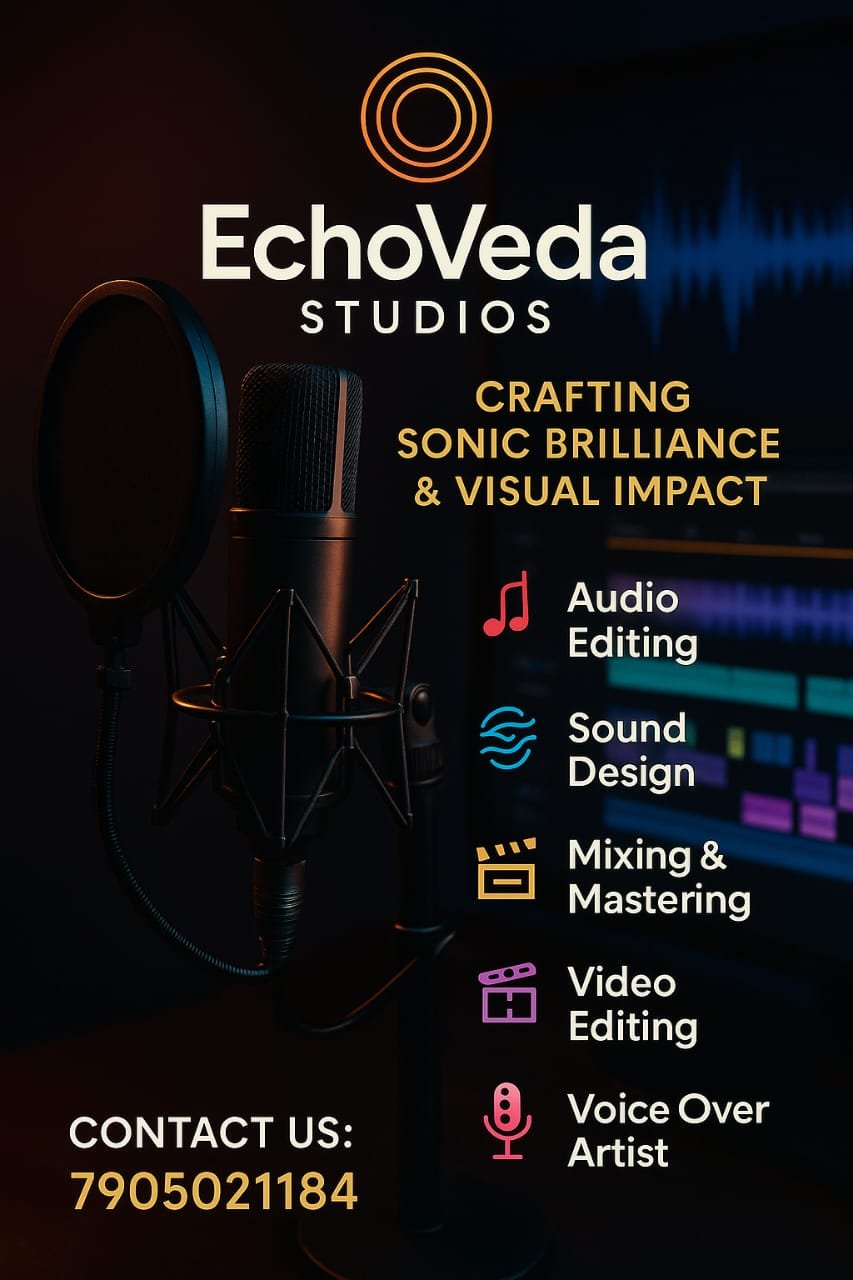
शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल के दौर में संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े जाने पर कड़ी असहमति जताते हुए इसे “सनातन की भावना का अपमान” बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले समेत कई नेताओं ने हाल के दिनों में इस भावना को दोहराया है, जिन्होंने हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति की आलोचना से अपनी सहमति जताई है।
Read More - प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया: यह जन-आंदोलन है
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए, जिससे भारत के आधारभूत दस्तावेज़ में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हालाँकि जनता सरकार 1978 में 44वें संशोधन के साथ इनमें से कई बदलावों को उलटने में कामयाब रही, लेकिन प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं हुआ।
प्रस्तावना और 42वां संशोधन
प्रस्तावना संविधान के लिए एक विज़न स्टेटमेंट के रूप में कार्य करती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में इन रे: द बेरुबारी यूनियन में अपने फैसले में उल्लेख किया था, यह संविधान के “निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी” है।
जब 1950 में संविधान को अपनाया गया था, तो प्रस्तावना में कहा गया था: “हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं” जो अपने सभी नागरिकों को “न्याय… समानता… स्वतंत्रता… और बंधुत्व” की गारंटी देगा।
1976 में तेजी से आगे बढ़ते हुए, 42वें संशोधन ने इसे “… संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य…” पढ़ने के लिए बदल दिया और बंधुत्व के वर्णन में “अखंडता” शब्द जोड़ा, जो अब “व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने” पर जोर देता है।
ये परिवर्तन 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई समायोजनों की एक झलक मात्र थे, जिसने मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय भी पेश किया, राज्य नीति पर नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया और परिसीमन पर रोक लगा दी।
इन बदलावों के पीछे
ये संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के राजनीतिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं, 21 महीने तक प्रधानमंत्री ने हुक्मनामा चलाकर शासन किया।
* 1950 के दशक से संसद और न्यायपालिका के बीच चल रहा संघर्ष भूमि सुधार के इर्द-गिर्द केंद्रित था। राजनीतिक वर्ग ने मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार के लिए न्यायालय के समर्थन को लोगों के सामूहिक अधिकारों पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देने के रूप में देखा।
इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से वामपंथी रुख अपनाया- 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त किया और उसी वर्ष बाद में "गरीबी हटाओ" ("गरीबी समाप्त करें") के नारे के साथ लोकसभा चुनाव जीते- "समाजवादी" शब्द को जोड़ने का उद्देश्य प्रधानमंत्री की आर्थिक दृष्टि के साथ संविधान के संरेखण को दर्शाना था।
42वें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि इस संशोधन का उद्देश्य “निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाना और उन्हें उन मौलिक अधिकारों पर वरीयता देना है, जिन पर सामाजिक-आर्थिक सुधारों को विफल करने के लिए भरोसा किया गया है…”।
* प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़ने के पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया था। हालाँकि, यह भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरने के साथ मेल खाता था।
1967 के आम चुनावों में, जनसंघ ने 35 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस की संख्या घटकर 283 रह गई। हालाँकि कांग्रेस ने 1971 में वापसी की, लेकिन जनसंघ आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक विरोधियों में से एक रहा, जिसके कई नेता, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे, जेल में बंद हो गए।
“हमारे संविधान और हमारे देश के संस्थापकों ने भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के रूप में देखा था… अब हम जो कर रहे हैं, वह बस इन आदर्शों को संविधान में शामिल करना है, जहाँ वे सही मायने में होने चाहिए,” इंदिरा ने लोकसभा में कहा।
* “अखंडता” शब्द को प्रस्तावना में उस समय पेश किया गया था जब इंदिरा का राजनीतिक प्रवचन - और आपातकाल के लिए उनका औचित्य - “राष्ट्र को विभाजित करने वाली ताकतों” के इर्द-गिर्द घूमता था।
“जब हम अखंडता की बात करते हैं, तो हम वास्तव में अविभाजित होने की गुणवत्ता या स्थिति का उल्लेख कर रहे होते हैं… एक राष्ट्र अपने लोगों और अपनी भूमि से मिलकर बनता है, और जब हम देश की अखंडता पर चर्चा करते हैं, तो हम देश की अविभाज्यता और राष्ट्र की एकता दोनों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं,” तत्कालीन कानून मंत्री एच आर गोखले ने विधेयक पर चर्चा करते हुए संसद में समझाया।
इन परिवर्तनों का प्रभाव
हालाँकि वे काफी हद तक प्रतीकात्मक थे, प्रस्तावना में किए गए बदलावों ने संविधान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन मामले में कहा था, “[प्रस्तावना] संविधान का हिस्सा नहीं है, और इसे कभी भी किसी भी मूल शक्ति का स्रोत नहीं माना गया है…”
धर्मनिरपेक्षता संविधान के विभिन्न प्रावधानों में एक आवर्ती विषय है। उदाहरण के लिए, यह अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समानता के अधिकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है। राज्य के खिलाफ ये सुरक्षा संविधान को मौलिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बनाती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इस दृष्टिकोण को मजबूत किया है। प्रस्तावना को संशोधित करने वाले 42वें संशोधन से पहले भी, 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में एक महत्वपूर्ण 13-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा की थी कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मुख्य विशेषता है जिसे हटाया नहीं जा सकता।
"राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए, को समाप्त नहीं किया जा सकता है," फैसले में जोर दिया गया।
1994 के बोम्मई मामले में, जिसमें केंद्र-राज्य संबंधों को संबोधित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता को संविधान के एक आवश्यक पहलू के रूप में पुष्टि की।
1980 में एक और महत्वपूर्ण निर्णय, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ने आपातकाल के दौरान किए गए संवैधानिक संशोधनों की भी जांच की। न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान निर्माताओं के लिए “समाजवाद” एक संवैधानिक आदर्श था, संविधान के भाग IV का संदर्भ देते हुए, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को रेखांकित करता है - एक गैर-प्रवर्तनीय ढांचा जिसमें कई समाजवादी अवधारणाएँ शामिल हैं।
“हमने खुद को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया, जिसमें हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का कर्तव्य शामिल है। इस प्रकार, हमने भाग IV को अपने संविधान में शामिल किया, जिसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विवरण दिया गया है जो उन समाजवादी लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं,” निर्णय में कहा गया।
नवंबर 2024 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान में “धर्मनिरपेक्षता” और “समाजवाद” को शामिल करने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बेंच ने कहा, "प्रस्तावना में किए गए बदलावों ने निर्वाचित सरकारों द्वारा अपनाए गए कानून या नीतियों को सीमित या बाधित नहीं किया है, जब तक कि वे मौलिक संवैधानिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए, हमें इस संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कोई वैध कारण नहीं दिखता..."
Business, Sports, Lifestyle ,Politics ,Entertainment ,Technology ,National ,World ,Travel ,Editorial and Article में सबसे बड़ी समाचार कहानियों के शीर्ष पर बने रहने के लिए, हमारे subscriber-to-our-newsletter khabarforyou.com पर बॉटम लाइन पर साइन अप करें। |
| यदि आपके या आपके किसी जानने वाले के पास प्रकाशित करने के लिए कोई समाचार है, तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें: 8502024040 |
#KFY #KFYNEWS #KHABARFORYOU #WORLDNEWS
नवीनतम PODCAST सुनें, केवल The FM Yours पर
Click for more trending Khabar

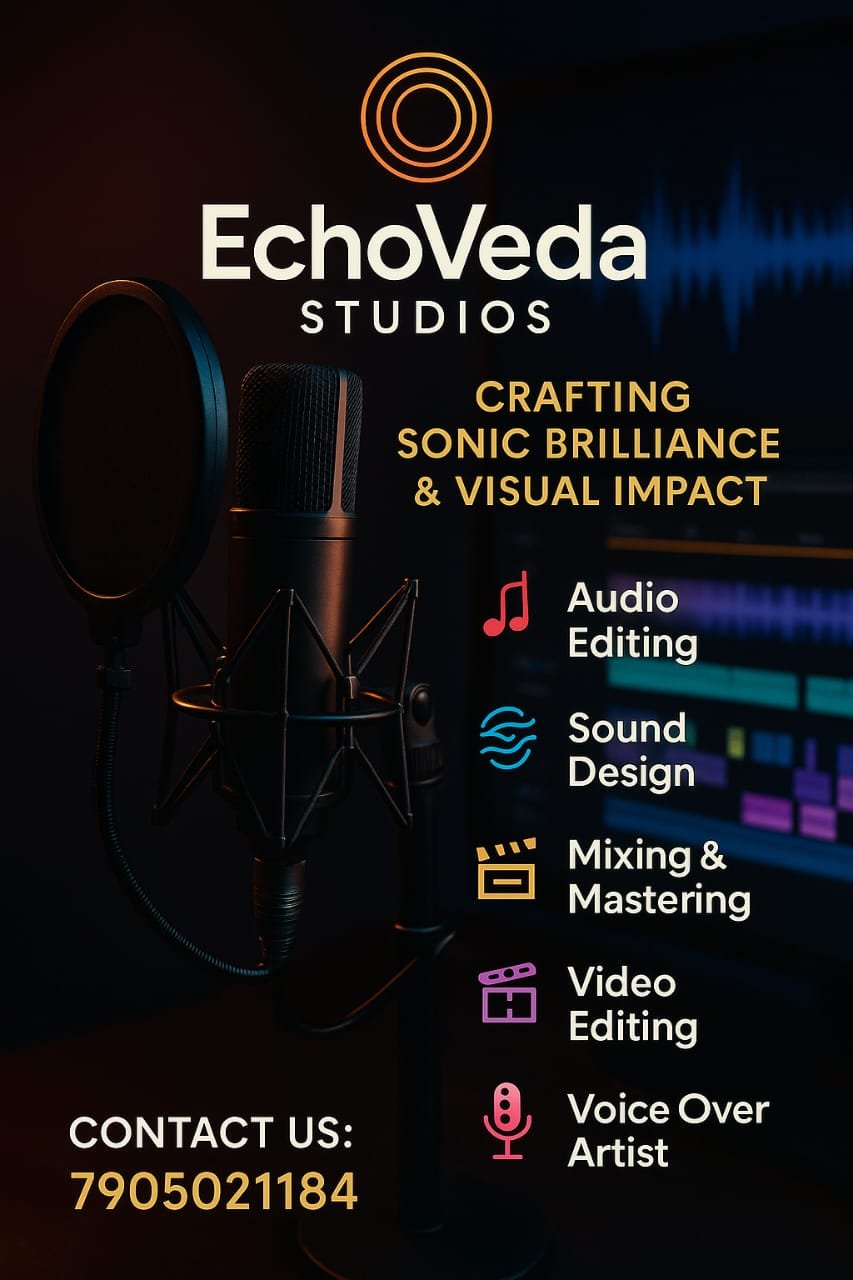
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Search
Category